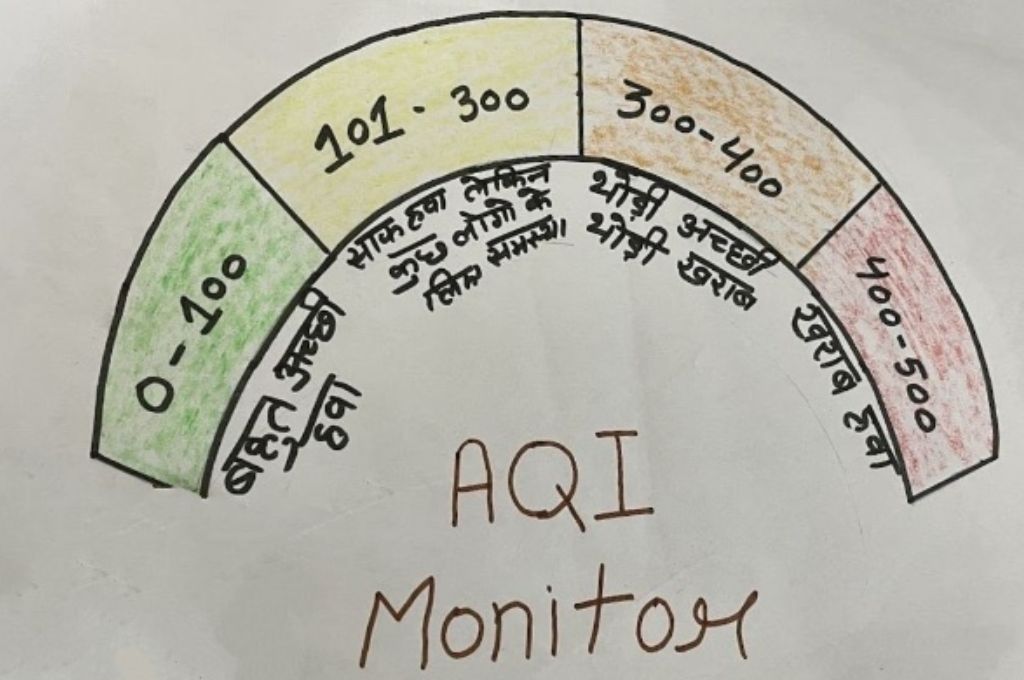क्या स्थानीय मोबाइल रिपेयर की दुकानें ई-कचरे को कम करने में मदद कर सकती हैं?

भारत में लंबे समय से पुरानी चीज़ों की मरम्मत और पुनःउपयोग कर उनके जीवनकाल को बढ़ाने का चलन रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी, अपसाइक्लिंग और थ्रिफ्टिंग जैसे शब्दों के वैश्विक स्तर पर प्रचलित होने से कहीं पहले से देश के लोग मोटे तौर पर कम खर्चे वाली टिकाऊ जीवनशैली अपनाते रहे हैं।
लेकिन फिर भी 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कंप्यूटर, स्मार्टफोन और छोटे आईटी उपकरणों से होने वाले ई-कचरे में 2010 से 2022 के बीच 163 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह दुनिया में सबसे अधिक वृद्धि दर है।
इसका एक प्रमुख कारण यह है कि पुराने मोबाइल, कंप्यूटर आदि उपकरणों की रिपेयरिंग या खरीद-फरोख्त में शामिल दुकानों को देश के ई-कचरे को कम करने की व्यवस्था में कहीं जगह नहीं दी जा रही है।
1990 और 2000 के दशक में ‘आईटी बूम’ के साथ ही देश भर में ऐसी दुकानों की संख्या बढ़ गई। आज भले ही ई-कचरे और पर्यावरण से जुड़ी नीतियों पर बातें हो रही हैं, लेकिन मीडिया की खबरों में रिपेयर करने वाली दुकानें और पुराने सामान बेचने वाले लोग ज़्यादा दिखाई नहीं देते।
रिपेयर का काम सीखना आसान नहीं
अशोक भूषण लगभग तीन दशकों से दिल्ली की चर्चित नेहरू प्लेस मार्केट में कंप्यूटर कॉमरेड्स नामक एक कंप्यूटर रिपेयर और रीसेल दुकान में टेकनीशियन के रूप में काम कर रहे हैं। अशोक के पास हार्डवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा था, लेकिन वह कहते हैं, “मैंने दुकान में शामिल होने के बाद रिपेयरिंग की कला सीखी। इससे पहले, मेरे पास बस किताबी ज्ञान था। वह भी उपयोगी है, क्योंकि फिर आप तेजी से काम सीखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप काम करते हुए ही सीखते हैं। “
त्रिपुरा के अगरतला में द मोबाइल स्टोर नाम की एक मोबाइल रिपेयर दुकान चलाने वाले राजेश भी अशोक की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। गौरतलब है कि नेहरू प्लेस भारत के प्रमुख रिपेयरिंग केंद्रों में से एक है। वहीं अगरतला अभी भी एक छोटा शहर है, जिसमें ग्राहकों की संख्या और संसाधन, दोनों ही सीमित हैं।
वह कहते हैं, “फेसबुक पर टेक इन्फ्लुएंसर सचिन कांबले के वीडियो देखने के बाद, मैंने अपने साले को सीपीयू की ट्रेनिंग के लिए नागपुर भेजा। लेकिन अब मुझे एक असेंबली मशीन, एक नए माइक्रोस्कोप वगैरह में निवेश करना होगा। इसमें 2-3 लाख रुपये का खर्च आएगा।, मैं आश्वस्त नहीं हूं कि क्या हम इस लागत को वसूल कर पाएंगे।”
अशोक और राजेश दोनों का मानना है कि यह एक अस्थिर उद्योग है, जहां न तो ग्राहक की मांग और न ही तकनीक एक अनुमानित पैटर्न पर चलती है। पहले, युवा और बुजुर्ग उपभोक्ता राजेश की दुकान पर स्क्रीन गार्ड या बैक कवर लगवाने आते थे, लेकिन अब वे यह काम खुद करने लगे हैं।
राजेश कहते हैं, “नए स्मार्टफोन की रिपेयर प्रक्रियाएं अब बहुत अधिक जटिल हो गई हैं। अब आपको तकनीक के हर हिस्से में में विशेषज्ञता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति डिस्प्ले को ठीक करना जानता है, हो सकता है वह सीपीयू के बारे में कुछ न जानता हो। पहले, यदि सीपीयू खराब हो जाता था, तो आपका फोन ईंट के समान बेकार हो जाता था।” जैसे-जैसे फोन महंगे होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे उनके पुर्जे भी महंगे होते जा रहे हैं। राजेश के अनुसार, अब अगरतला में पहले की तुलना में अधिक आईफोन उपभोक्ता हैं। एप्पल, गूगल और सैमसंग जैसी कंपनियों के प्रीमियम स्मार्टफोन भी मुश्किल रिपेयरिंग के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है की कंपनियां अक्सर इसके जरिए अपने उपभोक्ताओं कोहर कुछ वर्षों में नए फोन खरीदने के लिए मजबूर करती हैं।
राजेश जैसे छोटे शहरों के टेकनीशियनों के लिए राहत की बात यह है कि अब पुर्जे स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं। वरना पहले उन्हें दिल्ली से थोक में खरीदने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था।
डिस्पोजेबल टेक और आकांक्षी खरीदारों का युग
अशोक के अनुसार, निजी उपभोक्ता अगले नए गैजेट की तरफ आकर्षित होते हैं। “लोग नई तकनीक चाहते हैं, न कि ऐसी तकनीक जो लंबे समय तक चले। वे सस्ते कंप्यूटर खरीदते हैं जो कुछ वर्षों के भीतर काम करना बंद कर देते हैं। इससे भी ई-कचरे में वृद्धि हुई है।”
राजस्थान के चूरू में बालाजी लैपटॉप सोल्यूशंस नामक दुकान चलाने वाले चंद्रकांत अशोक कहते हैं, “अधिकांश लैपटॉप अब डिस्पोजेबल उत्पादों के रूप में बनाए जाते हैं।” चंद्रकांत यह बात इसलिए बखूबी जानते हैं क्योंकि वह छोटे शहर के ऐसे कई युवाओं को सेकंड हैन्ड कंप्यूटर बेचते हैं जो शिक्षा, नौकरी और मनोरंजन के लिए इन मशीनों पर निर्भर हैं।
यदि सरकार ई-कचरे को कम करने के तौर-तरीके में नवीनीकरण करना चाहती है, तो उन्हें चूरू और अगरतला जैसी जगहों पर ध्यान देना चाहिए। इन जगहों में तकनीक की मांग है, लेकिन बड़े शहरों की तुलना में जल्दी-जल्दी नए उत्पाद खरीदने की क्षमता कम है।
साहस संस्था की दिव्या कहती हैं, “भारत में एक बड़ा बढ़ता हुआ मोबाइल आकांक्षी वर्ग है, जो नवीनीकृत उत्पादों में रुचि रखता है बशर्ते उनकी गुणवत्ता अच्छी हो।” लेकिन वह इस बात पर भी जोर देती हैं कि रिपेयरिंग और नवीनीकरण के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती, है जो छोटे पैमाने पर महंगा साबित हो सकता है।

बालाजी लैपटॉप सोल्यूशंस जैसी तमाम स्थानीय दुकानें जयपुर और दिल्ली के बड़े इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन बाजारों के खिलाफ दौड़ में हैं, जिनके पास बहुत अधिक मानव संसाधन और बड़े संचालन केंद्र हैं। वहीं अर्बन कंपनी और कैशिफाई जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी समान सेवाएं बहुत सस्ते दर पर प्रदान कर रहे हैं।
ई-कॉमर्स के साथ मुक़ाबला
चूरू में लवली मोबाइल नामक दुकान चलाने वाले स्वराज ओझा की उम्मीदें स्थानीय लोगों के भरोसे पर क़ायम हैं। हालांकि, वे छूट और डील के उस मोहजाल से वाकिफ हैं, जो ई-कॉमर्स दिग्गज ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रदान करते हैं। “अब चूरू में भी कोई नया उत्पाद खरीदने में केवल कुछ क्लिक लगते हैं। सरकार को एक उचित मूल्य लागू करना चाहिए, ताकि हम जैसी दुकानें बाज़ार में बनी रह पायें।”
ऐसी ही कुछ स्थानीय दुकानों ने ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इंटरनेट को अपनाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें कुछ हद तक ही सफलता मिली है। दिव्या बताती हैं, “रिपेयर शॉप्स को गूगल मैप जैसे मंच पर पूरे संपर्क विवरण के साथ सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इससे उनकी पहुंच बढ़ेगी और उन्हें अधिक काम मिलेगा। इस गतिविधि के लिए सरकार और सीएसआर फंड का उपयोग किया जा सकता है।”
कंप्यूटर कॉमरेड्स ने जस्टडायल पर खुद को सूचीबद्ध कर एक समान प्रयोग किया था, जिसके नतीजे मिले-जुले रहे। “हमारे ग्राहक तो बढ़ गए, लेकिन हमें पूरे समय हज़ारों कॉल आने लगे। इससे हमारा काम बढ़ गया। हम सोचते थे कि क्या हमें कंप्यूटर ठीक करना है या कॉल का जवाब देना है?”
साहस संस्था द्वारा बैंगलोर में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, कई रिपेयर दुकान मालिकों का मानना था कि ग्राहक प्रोडक्ट वारंटी और लंबा चलने वाले रिपेयर के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर पर अधिक भरोसा करते हैं। वे ज़्यादा वारंटी के लिए ब्रांडों को भुगतान भी करते हैं।

इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ब्रांड रिपेयर और नवीनीकरण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। दिव्या कहती हैं, “कंपनियों को सरकार द्वारा निर्धारित नवीनीकरण लक्ष्य में भागीदार होना चाहिए। उन्हें नवीनतम उपकरणों में निपुण टेकनीशियनों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। सभी ब्रांड पूरे देश में ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए साथ पहल कर सकते हैं।”
पुरानी तकनीक कहां जाती है?
हमने जितने भी लोगों से बातचीत की, उन सभी में एक सामान्य विशेषता यह है कि उनका ई-कचरा रिसाइक्लिंग के लिए आउटसोर्स किया जाता है। ज्यादातर मामलों में, उन्हें नहीं पता था कि उनके कचरे को कौन रीसाइकल करता है। राजेश कहते हैं, “हर बार नए लोग होते हैं। कुछ कहते हैं कि वे दिल्ली से हैं और खराब पुर्जों और टुकड़ों को वहां ले जाकर उनपर काम करेंगे।”
बीते कई वर्षों में उन्होंने कचरा इकट्ठा करने की प्रक्रिया में भी बदलाव देखा है। “हम टूटे हुए डिस्प्ले को फेंक देते थे, जिसे अब कचरा संग्रहकर्ता ले जाते हैं। वह बताते हैं कि वो फ्लेक्स केबल को दिल्ली में स्थापनाओं को बेचते हैं, जिनके पास बॉन्डिंग मशीन होती है, जिसका उपयोग वे इन फ्लेक्स को नए डिस्प्ले से जोड़ने के लिए करते हैं।”
अध्ययनों से पता चलता है कि भारत का लगभग 90 प्रतिशत ई-कचरा अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा संसाधित किया जाता है। दिव्या कहती हैं, “खराब निगरानी और भ्रष्टाचार के कारण औपचारिक क्षेत्र से कचरा अनौपचारिक क्षेत्र में चला जाता है।” वे कहती हैं, “सीपीसीबी में कर्मचारियों की कमी है। जैसे-जैसे ई-कचरा बढ़ा है, वैसे-वैसे उनका काम का बोझ भी बढ़ा है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या इसके अनुपात में कम है। वे नगर पालिकाओं, प्लास्टिक, ई-कचरे जैसी तमाम चीजों की निगरानी करते हैं। ऐसे में वे ई-कचरे को कैसे प्रबंधित करेंगे?”
नेहरू प्लेस इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के पीछे स्क्रैप की दुकानें हैं। ये दुकानें चलन से बाहर और खराब गैजेट लेकर उन्हें पुर्जा-पुर्जा खोलते हैं और फिर उसे और अन्य स्क्रैप विक्रेताओं को बेचते हैं। इनमें से अधिकांश दुकानें लाइसेंसधारी और पारिवारिक व्यवसाय हैं, लेकिन वे अपने काम के अलावा ई-कचरा तंत्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। बैटरी और चिप्स से हानिकारक रसायनों के जोखिम के बावजूद, मशीनों के हिस्से अलग करने वाले व्यक्ति के पास अमूमन कोई भी सुरक्षा गियर उपलब्ध नहीं होता है।
ज्यादातर मामलों में लोगों को नहीं पता होता कि उनके कचरे को कौन रीसाइकल करता है।
हमारी बातचीत में एक विक्रेता ने बताया, “हम व्यक्तियों, दुकानों और यहां तक कि कंपनियों से भी खराब सामान लेते हैं। हम इसे वजन के आधार पर खरीदते हैं। फिर उसे बड़े डीलरों को बेचते हैं, जो धातुओं को पिघलाते हैं। हम उनके व्यवसाय के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। चूंकि नए गैजेट्स का वजन कम होता है, इसलिए पैसा कम होता है। लेकिन मैंने हमेशा यही काम किया है, इसलिए मैं इस व्यवसाय को जारी रखूंगा।”
इस ई-कचरे का अधिकांश हिस्सा सीलमपुर और मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। ये क्षेत्र असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने के लिए जाने जाते हैं और यहां कभी-कभी बाल श्रमिक भी पाये जाते हैं। सरकार ने ऐसे अनौपचारिक ठिकानों को औपचारिक बनाने की दिशा में बहुत कम किया गया है।
दिव्या एक वैकल्पिक मॉडल का सुझाव देती हैं, जो अनौपचारिक श्रमिकों को उनकी आय से वंचित नहीं करता है। “सरकार को अनौपचारिक क्षेत्र के परामर्श से सीलमपुर और मुरादाबाद जैसी जगहों पर ई-कचरा पार्क बनाने की आवश्यकता है, जहां अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा विभिन्न इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। यहां सरकार द्वारा सभी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा, भौतिक और प्रशासनिक, प्रदान किया जा सकता है।”
दिव्या कहती हैं, “यूरोपीय संघ के देशों की तरह, अधिकतर देशों को ब्रांडों को ऐसे उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिनसे कभी भी कचरा न पैदा हो। भारत में युवा लोगों का एक बढ़ता बाजार है, जो टिकाऊ तकनीक अपनाना चाहते हैं। सरकार इसका उपयोग नवीनीकरण मानकों को बेहतर बनाने के लिए कर सकती है।”
बेहतर डिजाइन किए गए उत्पाद कचरे को निश्चित तौर पर कम करेंगे। यदि सरकार और ब्रांड मॉड्यूलर फोन और असेंबल्ड कंप्यूटर बनाने पर काम करते हैं, तो उपभोक्ताओं की प्रवृत्ति स्थिरता की ओर बदल सकती है। इसके अतिरिक्त, इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि रिपेयर और रीसेल की दुकानें ई-कचरा कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहें, क्योंकि भारत की जानता का एक बड़ा हिस्सा आज भी अपने छोटे-बड़े कामों के लिए गली-मोहल्ले की दुकानों पर भरोसा जताते हैं।
इस लेख में सलोनी मेघानी ने भी योगदान दिया है।
—
अधिक जानें
- जानें, कैसे एक रेडियो अभियान के जरिए भारत ई-वेस्ट उत्पादन के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
- ई-वेस्ट की सुनामी: रीसाइक्लिंग की तुलना में पांच गुना तेजी से बढ़ रहा इलेक्ट्रॉनिक कचरा।
- देश में ई-कचरे के कलेक्शन और रीसाइकिलिंग के रीयल टाइम डाटाबेस को करना होगा मजबूत।
लेखक के बारे में
-
देबोजीत दत्ता आईडीआर में समपादकीय सहायक हैं और लेखों के लिखने, संपादन, सोर्सिंग और प्रकाशन के जिम्मेदार हैं। इसके पहले उन्होनें सहपीडिया, द क्विंट और द संडे गार्जियन के साथ संपादकीय भूमिकाओं में काम किया है, और एक साहित्यिक वेबज़ीन, एंटीसेरियस, के संस्थापक संपादक हैं। देबोजीत के लेख हिमल साउथेशियन, स्क्रॉल और वायर जैसे प्रकाशनों से प्रकाशित हैं।
-
राकेश स्वामी आईडीआर में सह-संपादकीय भूमिका मे हैं। वह राजस्थान से जुड़े लेखन सामग्री पर जोर देते है और हास्य से संबंधित ज़िम्मेदारी भी देखते हैं। राकेश के पास राजस्थान सरकार के नेतृत्व मे समुदाय के साथ कार्य करने का एवं अकाउंटेबलिटी इनिशिएटिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च मे लेखन एवं क्षमता निर्माण का भी अनुभव है। राकेश ने आरटीयू यूनिवर्सिटी, कोटा से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक किया है।
-
सृष्टि गुप्ता आईडीआर में एक सम्पादकीय विश्लेषक हैं और लेख लिखने, सम्पादन और अनुवाद से जुड़े काम करती हैं। इससे पहले सृष्टि ने स्प्रिंगर नेचर में संपादन से जुड़ा काम किया है। उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए किया है और लिंग, सामाजिक न्याय, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर शोध करने में रुचि रखती हैं।